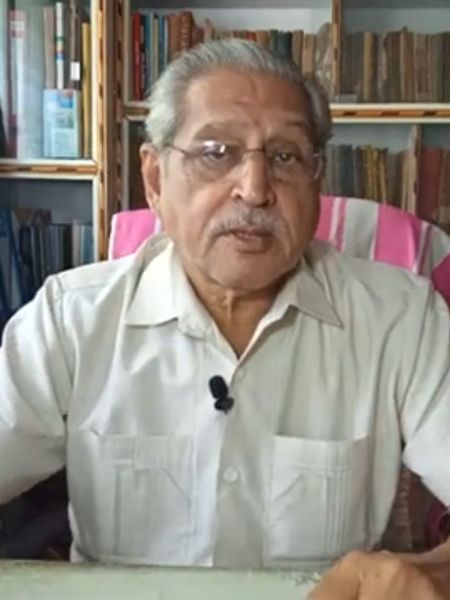लखनादौन
July 26, 2024
कोनी (बनाम कुण्डलगिरि)
July 26, 2024वाल्मीकि रामायण में पंपापुरी के सरोवर पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और हनुमान के मिलने का वर्णन मिलता है-
‘पश्य लक्ष्मण! पम्पायां वकं परं धार्मिकम्‘ राम के अयोध्या से चित्रकूट तक की यात्रा-काल में विन्ध्य के इन सघन वनों के भ्रमण का उल्लेख उपलब्ध है। बुंदेलखंड के वनों को कदाचित् इसीलिये प्राचीन काल से ‘रमन्ना’ अर्थात् रामारण्य (राम का वन) कहा जाता है। भारत के मध्यप्रदेश स्थित बुन्देलखंड के टीकमगढ़ जिला मुख्यालय से पूर्व दिशा की ओर लगभग पाँच किलो मीटर की दूरी पर यह ‘रमन्ना’ शुरू हो जाते हैं।
स्थिति
टीकमगढ़ पहुँचने के लिये मध्य रेलवे के ललितपुर स्टेशन से 45 किलोमीटर की दूरी, हर समय मिलने वाली बस या निजी वाहन से तय करना पड़ती है। टीकमगढ़ से 5 कि.मी. दूर स्थित पपौरा के पास ही एक झील है जो अब अत्यंत क्षीण स्वरूप में विद्यमान है, ‘पम्पा ताल’ कहलाता है और यहीं है भारत में समतल पर स्थित अद्वितीय मंदिरों का नगर पपौरा। पंपाताल बनाम पंपापुर का अपभ्रंश ‘पपौरा’ माना जाता है। अनुमानतः आस- पास के लोगों की दृष्टि से रामायण में वर्णित आम के वृक्षों से घिरे, कमलदल और मीन् आदि जल-जन्तुओं से परिपूर्ण पम्पापुर यहीं संभावित है।
स तां पुष्करिणीं गत्वा पद्मोत्पलझषाकुलाम् ।
रामः सौमित्रिसहितो विललापाकुलेन्द्रियः ।1।
(रामायणम् किष्किन्धाकाण्डम् प्रथम सर्ग)
समतल भूमि पर सर-कमलों से सुशोभित इस पम्पा झील पर राम के चरण पड़े थे। चूँकि कुछ ही दूर पर यहीं द्रोणगिरि (सेंधपा) भी स्थित है और कादम्बरी के साक्ष्य के अनुसार पम्पा सर दण्डकारण्य प्रदेश में ही होना चाहिए अतएव यदि यह अनुमानित तथ्य संभाव्य है तो पपौरा प्राकृतिक और पौराणिक, प्राचीन सौ से अधिक मंदिरों का यही नगर, वह पावन स्मारक होगा जहाँ भगवान राम ने सीता की खोज के लिये हनुमान से मंत्रणा की थी। संभव है भौगोलिकों की दृष्टि में, यह महज स्थानीय आत्मगौरव की कल्पना ही हो।
मंदिरों का मेला
भारत वर्ष में समतल पर स्थित इतनी अधिक संख्या में प्राचीन, विशाल और भव्य जिनालयों का एक साथ निर्माण अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। एक सौ आठ मंदिरों ने पपौरा में एक अपूर्व सुमेरु की रचना की है। देवालयों की इस शिल्प-मणिमाला में प्राचीन काल से वर्तमान तक की प्रचलित सभी मंदिर शैलियाँ संग्रहीत हैं यथा मुकुलित कमल, रथाकार, अट्टालिका, वरण्डा, मठ, मेरु, मानस्तंभ, चौबीसी, भौंयरे इत्यादि। यों पपौरा का शिल्प प्रमाणिक तौर पर, मैं बारहवीं-तेरहवीं सदी का मानता हूँ और यह निर्माण क्रम गत सदी में भी जारी रहा। तेरहवीं और पन्द्रहवीं सदी की तो अनेक भव्य प्रतिमायें प्रामाणिक शिलालेखों सहित दर्शनीय हैं। मंदिरों का प्रांगण पपौरा, देश में अपनी तरह का विशिष्ट जिन-तीर्थ है। एक बड़े क्षेत्रफल में केवल मंदिर ही मंदिर हैं, आबादी यहाँ नहीं के बराबर है।
पाहन, पानी और पादपमयी पपौरा
चारों ओर प्रकृति की अद्भुत छटा बिखरी पड़ी है। आम, महुआ, अचार, कंजी, चिरौल, बाँस, सेमर और जामुन के हरे-भरे वृक्ष गलवहियाँ डाले पपौरा मार्ग पर बन्दनवार बनाकर आपका स्वागत करेंगे। करोंदी की गंध, मौलश्री के रंग-बिरंगे सुमन और मोर कोयल का नृत्य संगीत आपको लुभाये बिना नहीं रहेगा। टीकमगढ़ छोड़ते ही पपौरा की ओर दृष्टिपात करने पर आपको गगन चुम्बी जिन मंदिरों की शिखर पंक्ति के दर्शन, पुलकित करने लगेंगे। पहुँचते ही सामने से विशाल रंगीन पाषाणी रथ, घोड़ों पर जैसे दौड़ता सा प्रतीत होता है। यह विलक्षण रथाकार रचना वस्तुतः एक पूर्ण मंदिर को ही, पपौरा के प्रमुख प्रवेश द्वार पर वास्तुकार द्वारा प्रदान की गई है जो विस्मयकारी है। प्रकृति के पावन आँचल में बसे पपौरा में पाहन, पानी और पादक का मनोहारी समन्वय है।
शिल्प का सुगढ़ सौन्दर्य
मध्ययुगीन वास्तु शिल्प का पपौरा केन्द्र बिन्दु है। चारों दिशाओं में तीर्थस्थल और कला केन्द्र अवस्थित हैं-खजुराहो, देवगढ़, बानपुर, ओरछा, चित्रकूट, द्रोणागिरि, अहार, कुण्डलपुर, पन्ना और कालिंजर आदि। तीर्थगज की भाँति बहुसंख्य और उत्तुंग मंदिरों का गढ़ पपौरा, चूना, मिट्टी और देशी पत्थर के वाग्नु निर्माण का अपनी तरह का अनोखा कला केन्द्र है। आम पास के विभिन्न पुरातात्त्विक स्थलों पर पपौरा का अद्भुत प्रभाव पड़ा है। पपौरा की पावनता है यहाँ की प्राचीनता में, प्रांजलता है यहाँ के पौराणिक आख्यानों में और पुलक है पानीदार पाषाणों में। परन्तु पपौरा के सभी मंदिरों की चर्चा करना जहाँ इस लघु निबंध में संभव नहीं है, वहीं मंदिरों के संसार से कुछ विशेष का वर्णन हेतु चयन भी असमंजस उत्पन्न करता है। तथापि कुछ विशिष्ट विम्बों पर दृष्टि केंद्रित करना आवश्यक है।
प्राचीन समुच्चय
एक मंदिर के चारों ओर स्थित बारह प्राचीन मठों के सृजन से तीर्थकर के समवशरण जैसी बारह सभाओं की संरचना दर्शनीय है। किंवदन्तियों की कतिपय अन्तर्कथायें पौराणिक परम्पराओं में आ गई हैं। कुछ तो ऐसे प्रमाण विद्यमान हैं कि वैज्ञानिक मस्तिष्क भले न माने पर आस्थावान हृदय समर्पित हुये बिना नहीं रहते। ऐसा ही एक पारम्परिक कथानक है पपौरा का पतराखन कुआँ। यह कुआँ आज भी अपना उदार और आपूरित आंचल फैलाये मानव पयस्वनी बनने हेतु आतुर सा दिखता है, जिसने अतीत में अनेक प्राणियों की प्राण रक्षा की है।
कहते हैं संवत् 1872 में निकटवर्ती छतरपुर की एक पुण्य प्रबल वृद्धा ने पपौरा के, वर्तमान प्रथम जिनालय की प्राण-प्रतिष्ठा में पंचकल्याणक समारोह आयोजित कराया। दूर-दराज के असंख्य श्रद्धालु एकत्रित हुये। सभी व्यवस्थाएँ पूर्ण थीं। मेले की रंगीनी में, धर्म की सहज साधना युक्त साधु-साध्वियाँ और जप-तप का कार्य प्रारंभ, पर अनायास ही अप्रत्याशित भीड़ की उपस्थिति और मौसम की अनुदारता ने मेले में पानी का अभाव पैदा कर दिया। ‘बिन पानी सब सून’ चारों ओर त्राहि-त्राहि की स्थिति और वृद्धा के आयोजन पर टीका टिप्पणी। समाज भला किसे बख्शता है? कोई उसके धन पर कोई मन पर आक्षेप करने लगा। वह समय, कार्य पर नहीं धर्म पर आस्थित तो था ही, वृद्धा कातर हो उठी। क्षेत्रीय बुजुर्गों से, वृद्धा ने तीर्थ के सबसे बड़े कुएँ के पास चलने को कहा और उसे कुएँ में उतारने का आग्रह किया। भला कौन उसे कुएँ में भेजने का कलंक लेता ? पर बुढ़िया जिद पकड़े थी कि उसे कुएँ की तलहटी में संन्यास लेना है। यदि नहीं उतारोगे तो वह स्वमेव कूद पड़ेगी। पदाधिकारियों ने मजबूर होकर वृद्धा को एक चौकी पर बैठाकर कुएँ में रस्सी के सहारे उतार दिया। पुण्यात्मा ने कुएँ में उतरकर संन्यास धारण किया और सर्वमान्य ‘णमोकार मंत्र’ का प्रभावी जाप प्रारंभ किया। आस्था प्रस्फुटित हुई, णमोकार मंत्र का जाप जैसे जैसे पूर्ण हुआ, कहते हैं कुएँ में जल स्रोत फूट पड़ा और पानी का तल बढ़ता गया। जन समूह जय जयकार कर रहा था और वृद्धा महिला तपस्विनी जैसी चौकी पर, पानी के बढ़ते तल पर आरूढ़ कुएँ में ऊपर उठती आ रही थी। कुआँ भरा ही नहीं बल्कि पानी बाहर बहकर मेले में प्रवाहित होने लगा और जल प्लावन की स्थिति बनती सी लगी। जन समूह में फिर चीख पुकार, तब कुएँ की जगत पर तपस्विनी वृद्धा ने पुनः वीतराग भगवान की आराधना की और जल प्रवाह ठहर गया।
उपर्युक्त अतिशय की किंवदन्ती पपौरा के उन अनेक चमत्कारों में में एक है, जिसके कि कारण इस क्षेत्र को अतिशय क्षेत्र ‘पपौरा’ कहा जाता है। यह ‘पतराखन कुआँ’ आज भी पपौरा में श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र है। पतराखन अर्थात् प्रतिज्ञा की लाज या अवसर पर प्रण रखने वाला, मान रखने वाला। मैं तो सम्पूर्ण क्षेत्र को ही जैन समाज ही नहीं मानवता का पतराखन पपौरा मानता हूँ। मेरा बचपन पपौरा के मेले के कवि सम्मेलनों में खूब फुदका है। यद्यपि इस तरह की अनेक किंवदंतियाँ पपौरा के बारे में लोगों की जुबान पर हैं। पर प्रमाणिकता के अभाव में, मैं इन्हें आस्था की अति ही मानता हूँ। एक विशाल बावड़ी भी यहाँ दर्शनीय है। लोग कहते हैं कि कुछ दशकों पूर्व तक यह बावड़ी श्रद्धालु पर्यटकों को माँगने पर बर्तन आदि प्रदान करती थी, जिन्हें भोजनादि से निवृत्त होने पर उसी बावड़ी में वापस कर दिया जाता था। पर किसी विधर्मी की नियत बिगड़ गई और जब बावड़ी को बर्तनादि वापस नहीं दिये तो बावड़ी का ‘सत्व’ जाता रहा। यह कहाँ तक सच है, यह तो मुझे नहीं मालूम पर इतना अवश्य ज्ञात है कि पर्यटकों को आज भी पपौरा की धर्मशालाओं में वे सभी सुविधाएँ निःशुल्क प्राप्त हैं जो कि दो-चार दस दिन तक ठहरने के लिये किसी भी परिवार को अपने घर में दैनंदिन जीवन के लिये आवश्यक होती हैं। विशाल लम्बी चौड़ी धर्मशालायें, आधुनिक सुविधा युक्त विश्राम गृह और परिवहन की उपयुक्त व्यवस्था पपौरा में दर्शनार्थियों को आज सुगमता से उपलब्ध है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रप्रसाद जी ने पपौरा को देखकर जो स्वप्न संजोये थे, बुंदेलखण्ड के आध्यात्मिक गांधी जैसे मान्य श्री गणेश वर्णी जी की आकांक्षाओं को हम पपौरा में साकार कर सकते हैं। यदि धर्म की रूढ़ियों से हम किंचित् भी ऊपर उठ सकें, गजरथ व मेलों में ही धर्म की इतिश्री न समझें और साथ ही वैयक्तिक या दलवादी स्वार्थों से ऊपर उठकर पपौरा को बुंदेलखण्ड का ‘शान्ति-निकेतन’ बनाने पर सम्यक् दृष्टि से विचार करें, तो यह सपना साकार होना असंभव नहीं है।