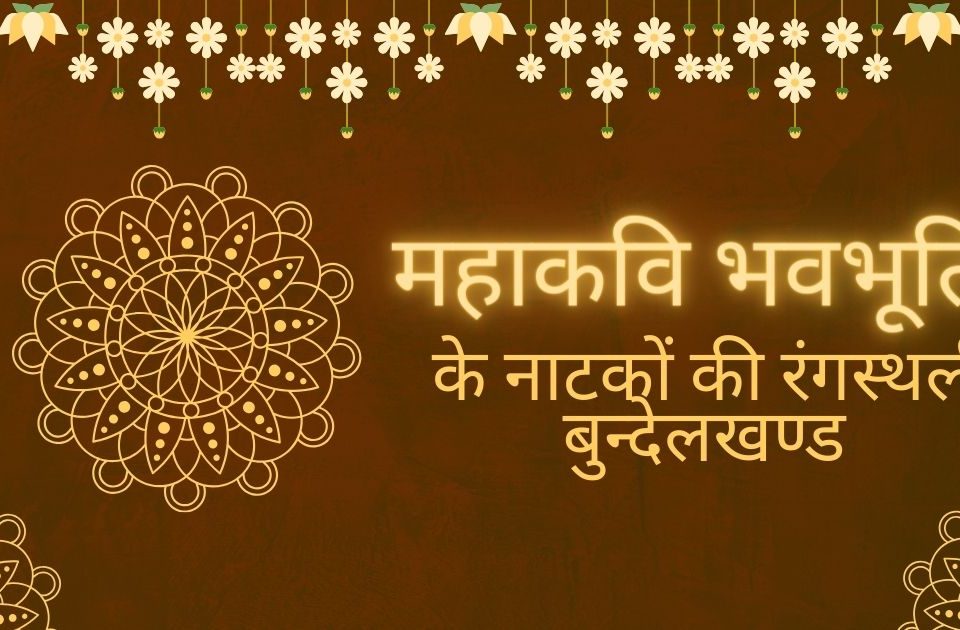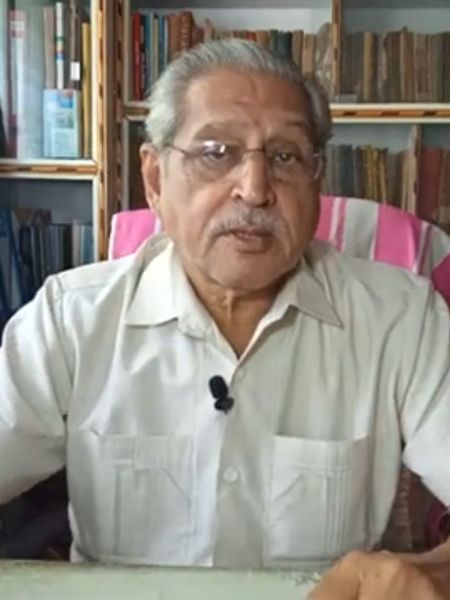महाकवि भवभूति के नाटकों की रंगस्थली बुंदेलखंड
June 14, 2024
सामाजिक लोक नृत्य
June 24, 2024डॉ. रामेश्वर प्रसाद गुप्त
बुंदेलखंड की सीमा विषयक श्री वियोगी हरि का प्रस्तुत दोहा प्रायः सर्वमान्य है:
“इत यमुना उत नर्मदा, इत चम्बल उस टौंस ।
छत्रसाल सौं लड़न की, रही न काहू हौंस ।।”
उक्तानुसार उत्तर में मुरैना, भिन्ड, ग्वालियर तथा जालौन से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद, बैतूल, छिन्दवाड़ा तथा बालाघाट तक एवं पूर्व में बाँदा, सतना, पन्ना, जबलपुर तथा मन्डला से लेकर पश्चिम में गुना, विदिशा तथा रायसेन तक विस्तृत मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के लगभग अट्ठाईस जिलों का क्षेत्र बुंदेलखंड की पावन धरान्तर्गत है।
इस बुंदेलखंड में सृष्टि रचयिता ब्रह्मा के पुत्रों- सन्क, सन्न्दन, सनातन, तथा सन्त्कुमार ने जहाँ दतिया जिले के शिवधाम सेवढ़ा को अपनी तपस्थली बनाया, वहीं मंत्रदृष्टा महर्षियों अगस्त्य, भारद्वाज, गालव, जाबालि आदि ने देववाणी में वेदमंत्रों का उद्घोष कर इस भूमि को परम पावन किया गालव ऋषि का गोपाचल अधुना ग्वालियर तथा जाबालि ऋषि का जाबालिपुरम् अधुना जबलपुर उक्त ऋषियों द्वारा संस्कृत विद्यापीठों एवं उनकी कालगुप्त संस्कृत संरचनाओं के अन्वेषण के प्रति आज भी विद्वानों के मानस को उत्प्रेरित करते हैं।
संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि की पावन कृति “रामायण” के अध्ययन से स्पष्ट है कि “भारत” की हृदयस्थली बुन्देलभूमि के अनेक स्थलों का उन महाकवि ने सुचारू एवं सूक्ष्म वर्णन किया है। इससे यह सुप्रतीत है कि आदिकवि ने भी इस धराधाम को अपनी कर्मस्थली बनाया होगा।
अष्टादश पुराणों के रचयिता महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास ने तत्कालीन “अधिराज” नाम से प्रख्यात दन्तवक्य की नगरी “दतिया” से लेकर दन्तवक्र के भाई शिशुपाल की चन्देरी तक के सम्पूर्ण क्षेत्र का हस्तामलक वर्णन किया है। इसी प्रकार उन महर्षि ने इस प्रखण्ड में स्थित माहिष्मती आदि अन्यान्य पुरियों तथा तत्कालीन राज्यों एवं वनों, उपवनों, आश्रमों आदि का भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म वर्णन किया है, जिससे स्पष्ट है कि उन सिद्धकवि ने इस प्रदेश के अनेक स्थलों का भ्रमण कर अपने काव्यकर्म को पूर्ण करने में चिरकाल तक यहाँ विश्राम किया होगा।
संस्कृत के सरस एवं रससिद्ध महाकवि कालिदास द्वारा इसी क्षेत्र के दशार्ण जिसकी राजधानी विदिशा थी का सुचारू, सुस्पष्ट एवं सहज वर्णन प्रमाणित करता है कि उक्त महाकवि ने अवश्य ही इस क्षेत्र में पदार्पण कर अपने कार्य की गतिशीलता में इसका महनीय योग लिया होगा। इस बुन्देलधरा से सम्बद्ध रहे अन्य संस्कृत महाकवि भवभूति, मण्डन मिश्र एवं उनके साथ माहिष्मती के ही अनर्घराघव के रचयिता कवि “मुरारि”, यो मध्यदेशे निवसति स कविः सर्वभाषानिष्णः का अपनी कृति “काव्य मीमांसा” में उल्लेख कर अपने को इसी क्षेत्र से सम्बन्धित कहने वाले “जबलपुर” के समीप “त्रिपुर” तेवर प्राम के मान्य दशम शताब्दी के आचार्य राजशेखर आदि विश्रुत हैं।
मध्ययुगीन हिन्दी के आचार्य एवं महाकवि केशव की रामचन्द्रिका का आधार संस्कृत की अनेक काव्य कृतियाँ रहीं है। इससे उक्त महाकवि की संस्कृत काव्य सर्जना की गति अनुमानित होती है। भले ही उनकी संस्कृत रचनायें अलिखित रही हों। सगुणोपासक भक्तकवि गोस्वामी तुलसीदास का प्रचुरकाव्य कर्मकाल इसी बुंदेलखंड के चित्रकूट धाम में व्यतीत हुआ था। उन्होंने रामचरित मानस के प्रत्येक काण्ड के प्रारम्भ में प्रसादगुणयुक्त सुललित संस्कृत भाषा के माध्यम से अपने संस्कृत काव्य को मूर्धन्य स्थान दिया है तथा “मानस” के मध्य में भी अनेक स्थलों पर सरस, सरल, संस्कृत काव्यावलियों को पिरोकर इस धराधाम से सम्बद्ध संस्कृत कवि होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है।
बुंदेलखंडके उत्तरभूभाग के गोपाचल ग्वालियर में मध्ययुग में तोमर राजाओं के समय संस्कृत साहित्य की अपरमित सृष्टि हुई। तोमरवंशीय शासक वीरसिंह देव ने सन् 1382 ई में वैद्यक ग्रन्थ की संस्कृत में संरचना की। पन्द्रहवीं शताब्दी में भट्टारक गुणकीर्ति के आश्रयदाता श्री कुशराज के आग्रह से “पद्मनाथ” कायस्थ ने संस्कृत में “यशोधरचरित” महाकाव्य की रचना की। महाराज वीरमदेव के राज्यकाल में लगभग सन् 1410 ई में नयचन्द्र सूरि ने संस्कृत में “हम्मीर महाकाव्य” की रचना की। इसीकाल में “नयचन्द्र सूरि” ने “रम्भामंजरी” सट्टक की भी रचना की।
डूंगरेन्द्र सिंह तोमर राज्यकालीन जैन महाकवि श्री “रदधू” ने पंद्रहवीं शताब्दी में अपभ्रंश काव्य “पदमपुराण” की रचना की। गोपांचल के ही श्री कल्याण सिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में संस्कृत में “अनंगरंग” प्रन्थ का प्रणयन किया। इनकी अन्यकृति ‘सुलैमल्लचरितम” भी उल्लेखनीय है। गोपाचल के उन्नीसवीं शताब्दी के संस्कृत साहित्यकार श्री सोमनाथ शास्त्री वाडेकर, श्रीबाल शास्त्री गर्दे, श्री बालशास्त्री रानाडे, श्री रघुपति शास्त्री बाजपेयी, श्री दामोदर शास्त्री भरद्वाज, श्री रघुनाथ शास्त्री वेलणकर, श्री विष्णुराम दीक्षित, श्री वठ्ठल बुधकर, श्री पर्वगीकर, श्री सदाशिव शास्त्री, मुसलगाँवकर, आदि उल्लेख्य हैं।
बीसवीं शताब्दी के गोपाचल के संस्कृत साहित्यकारों में डॉ. हरिराम चन्द्र दिवेकर, डॉ. गोविन्दराम मराठे, डॉ. राजाराम गाडगिल, डॉ. शिवशरण शर्मा द्विवेदी इन्होंने “जागरणम् एवं अन्यान्य संस्कृत काव्यकृतियों की संरचना की आदि उल्लेखनीय है।
संस्कृत हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. प्रभुदयाल अग्निहोत्री का भी अधिकांशतः साहित्य सर्जना का कार्यकाल गोपाचल (ग्वालियर) ही रहा है। ग्वालियर के एक अन्य संस्कृत साहित्यकार श्री मोहन गुप्त (राजस्व मण्डल, ग्वालियर) ने “मैकवैघ” का संस्कृत पद्यानुवाद “मैधवघ” शीर्षक से मधुर एवं ललित शैली में रचनाकर संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि की ।
ग्वालियर संभाग में स्थित दतिया जिले के उन्नीसवीं एवं बीसवीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत साहित्यकारों में “श्री सौन्दर्यसागरः” काव्य के रचयिता पं. श्री राधालाल गोस्वामी, श्री बालकृष्ण शास्त्री तैलंग, “श्री प्रेमनारायण गोस्वामी, चरितमृतम” के रचयिता श्री अयोध्या प्रसाद उपाध्याय “घटिकाशतक”, पं. नारायणदास वैद्य “शिरधर, पं. गोविन्द दास दीक्षित, पं. रामचरण मिश्र, पं. कमलापति लिटौरिया, पं. मुकुन्दलाल सिद्धू, पं. छोटेलाल गोस्वामी, पं. कण्ठमणि शास्त्री तेलंग, पं. रामदयाल शास्त्री, म.प्र. शासन् से सम्मानित संस्कृत के महाकवि पं. सुधाकर शुक्ल इनके तीन संस्कृत महाकाव्य उपलब्ध है- भारतीस्वयम्बरम। गाँधी सौगन्धिकम् अप्रकाशित तथा स्वामिचरित चिन्तामणिः प्रकाशित। इनके अतिरिक्त “आर्यासु’ पन्द्रह सौ आर्याछन्दों की रचना तथा देवदूतम प्रकाशित एवं अनेक स्फुट संस्कृत रचनायें उपलब्ध हैं। पीताम्बरापीठ महाराज, पं. रामेश्वर शास्त्री, श्री महेश मिश्र “मधुकर” आदि प्रगण्य एवं उल्लेखनीय है।
बुंदेलखंड के “सागर” तथा जबलपुर सम्भागों में संस्कृत साहित्य की अनवरत सृष्टि उल्लेख्य है। अपनी सेवा का अधिकांश समय सागर में व्यतीत कर संस्कृत साहित्य की समृद्धि में महत योग प्रदान करने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. रामजी उपाध्याय आचार्य एवं विश्रुत साहित्यकार डॉ. बच्चूलाल अवस्थी, साहित्यिक प्रतिभा से प्रसिद्धि प्राप्त डॉ. रेवाप्रसाद द्विवेदी, अनेक संस्कृत काव्यों के रचयिता डॉ. राधावल्लभ त्रिपाठी, डॉ. श्रीमती वनमाला भवालकर, श्री प्रेमनारायण द्विवेदी आदि को संस्कृत, आधुनिक संस्कृत साहित्यकारों में विश्रुत एवं विशिष्ट स्थान प्राप्त है। जाबालिपुरम (जबलपुर) के आधुनिक संस्कृत साहित्यकार पं. लोकनाथ शास्त्री, श्री गोविन्द विश्वास भावे, डॉ. कृष्णकान्त चतुर्वेदी, डॉ. रहस बिहारी द्विवेदी आदि विश्रुत हैं।
सत्रहवीं शताब्दी में ओरछा नरेश वीरसिंह के सान्निध्य में संस्कृत की श्री वृद्धि करने वाले गोपाचल में जन्मे मित्रमिश्र ने अनेक संस्कृत कृतियों का प्रणयन किया। इनकी “वीरमित्रोदय” संस्कृत रचना अति प्रसिद्ध है। इनकी अन्य रचनाओं में “आनन्दकन्दचम्पू” वीरमित्रोदय गणित प्रन्थ याज्ञवल्क्य स्मृति टीका आदि भी हैं।
बुंदेलखंड के अन्य ख्याति प्राप्त संस्कृत साहित्यकारों में महामहोपाध्याय पं. मथुरा प्रसाद दीक्षित जन्म संवत् 1930 वि. हरदाई कार्यकाल झाँसी ने लगभग तीस कृतियाँ संस्कृत साहित्य को देकर संस्कृत साहित्यकोष की अपूर्व वृद्धि की। झाँसी संभाग के परगना तालबेहट निवासी “श्री रामस्वरूप शास्त्री” “अमर” ने भी संस्कृत में अनेक गीतों का सर्जन कर संस्कृत साहित्य को अपना योगदान किया।
बुंदेलखंड के पालि प्राकृत और संस्कृत के शिलालेखों तथा ताम्रपत्रों ने भी संस्कृत साहित्य को योग दिया। ग्वालियर गुजर्रा (दतिया), नरवर, जबलपुर, खजुराहो, रानोद आदि के शिलालेख इसके प्रमाण हैं।
निष्कर्षतः प्राचीनकाल से यह प्रसिद्ध क्षेत्र, जो कि मध्यकाल में बुंदेलखंड नाम से महनीय कीर्ति को प्राप्त हुआ, संस्कृत साहित्य सर्जना में अपनी अबाध गति बनाये हुये है। महान देश भारत की यह हृदयस्थली संस्कृत साहित्य की सर्जना में अनवरत योग करती रहेगी, ऐसा विश्वास है।